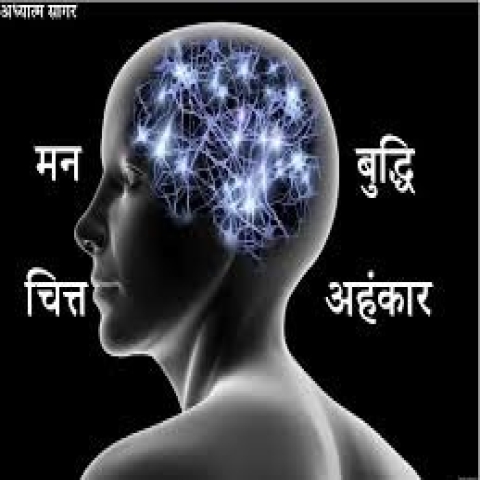
Spiritual Foundations of Indian Education – Part Three (Conscience and its Education)
भारतीय शिक्षा के आध्यात्मिक आधार – भाग तीन (अन्तःकरण व उसकी शिक्षा)
– ब्रज मोहन रामदेव
करण अर्थात् उपकरण या साधना। ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन है। 1. बाह्य करण 2. अन्तः करण। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां बाह्य करण है। हाथ, पैर, वाणी, वायु और उपस्थ कर्मेन्द्रियां है। तथा आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा ज्ञानेन्द्रियां है। अन्तःकरण के अन्तर्गत मन, बुद्धि, अंहकार तथा चित आते हैं। मन का कार्य विचार करना है। बुद्धि विवेक करती है, अंहकार कर्तापन व भोलापन का अनुभव कराता है तथा चित संस्कार ग्रहण करता है। बातों को स्मृति में रखने का कार्य चित करता है। अन्तःकरण के शुद्ध होने से चित पर संस्कारों की छाप पड़ती है। शुद्ध अंतःकरण की अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा व अभ्यास से अन्तःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा के इन चारों का विवरण निम्न प्रकार से हैं –
मन : मन भावों का भण्डार है जो घटते-बढ़ते रहते हैं, इसलिये मन को सोम या चन्द्रमा कहा गया है। यह भारतीय मनोविज्ञान की छटी ज्ञानेन्द्रिय है। मन विचार करता है, इच्छा करता है और भावों को अनुभव करता है। मन की गति सृष्टि में सबसे अधिक है। यह बिना किसी अवलम्बन के जहां चाहे वहां पहुंच जाता है। पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय को वश में रखने वाला व कार्य में प्रवृत करने वाला मन है। मन को शांत, एकाग्र व अनासक्त करना मन का विकास करना है। मन का प्रभाव एक और शरीर पर पड़ता है तो दूसरी ओर बुद्धि पर पड़ता है। मन जब तक शांत और एकाग्र नहीं होगा, बुद्धि सही ढ़ंग से अपना कार्य नहीं करेगी। बुद्धि का कार्य प्रशस्त करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। मन को विभिन्न उपायों यथा- संयम, ध्यान, शुद्ध आचार-विचार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इन षडरिपुओं से मुक्त करना तथा मन को एकाग्र व अनासक्त बनाना आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।
बुद्धि : बुद्धि का काम जानना है। ज्ञान शब्द बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से निरीक्षण परीक्षण करती है, संश्लेषण, विश्लेषण करती हैं। तर्क व अनुमान करती है तथा विवेक व निर्णय करती है। प्रतिभा, मेधा, धी आदि सभी बुद्धि के ही विभिन्न रूप हैं। बुद्धि अपना विवेक व निर्णय ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिये मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। मन यदि ठीक रहा तो बुद्धि भी ठीक रहती है। बुद्धि को तीक्ष्ण, शुद्ध व ग्रहणशील बनाने के लिये मन की एकाग्रता, शांति व अनाशक्ति आवश्यक है। बुद्धि, मन को अपने वश में करे और स्वयं आत्मनिष्ठ बने तो ज्ञानार्जन का काम ठीक होता है। बुद्धि का संबंध एक ओर मन के साथ होता है। तो दूसरी ओर चित के साथ होता है। मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना, बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। योग के अष्टांग मार्ग द्वारा मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाया जा सकता है। बुद्धि हमें सोचने व विकल्प चुनने में सहायता करती है। बुद्धि के ठीक होने के लिये मन का ठीक होना आवश्यक है।
अंहकार : अंहकार की अभिव्यक्ति ‘मैं’ द्वारा होती है। यह आत्मा को शरीर के साथ ‘मैं’ के रूप में पहचानता है। यह व्यक्ति केन्द्रित है, जिसके चारों ओर व्यक्तित्व का गठन होता है। अंहकार लोकेषण तथा लोक प्रसिद्धि की आंकाक्षा को जन्म देता है। प्रतयेक क्रिया का कर्ता अहंकार होता है। जैसे – “यह कार्य मैंने किया” आदि। यह कर्ता और भोला दोनों है। अंहकार क्रिया करने का निर्णय शुद्धि के साथ मिलकर लेता है। अंहकार जब आत्मनिष्ठ होता है तब यह सकारात्मक बन जाता है तथा दायित्व बोध अनुभव करता है। दायित्व बोध से ही कार्य की सार्थकता प्राप्त होती है। अंहकार हमें अपनी पहचान का एहसास कराता है। बुद्धि अंहकार से पोषण प्राप्त करती है। अंहकार की धुरी पर ही बुद्धि काम कर सकती है।
चित : चित शुद्ध प्रज्ञा तथा चेतना होती है। जो स्मृतियों से पूरी तरह मुक्त रहती है। आत्म तत्व का यह सबसे पारदर्शी आवरण है। यह आत्मतत्व के प्रकाश से आलोकित है। मनुष्य के व्यक्तित्व की यह सबसे प्रगत अवस्था है। चित पर सभी प्रकार के संस्कार होते हैं। चित पर पूर्वजन्म के संस्कार भी होते हैं और अनुवांशिक संस्कार भी होते हैं। इन संस्कारों से चित को मुक्त करना ही चित को शुद्ध करना है। चित जब शुद्ध रहता है तो साफ दर्पण के समान रहता है, जिसमें आत्मतत्व स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है। जब विभिन्न प्रकार के संस्कारों से मुक्त रहता है। धूल की परत से छाये हुए दर्पण के समान रहता है, जिसमें आत्मतत्व का प्रतिबिम्ब अस्पष्ट दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता। इसलिये चित को शुद्ध करना चाहिये।
अन्तःकरण का यह भाग व्यक्ति को याद रखने या भूलने से संबंधित है। क्रिया, संवेदना, विचार, विवेक आदि सभी चित पर संस्कार अंकित करते हैं। चित पर संस्कार होने से ही किसी भी कार्य या अनुभव की स्मृति बनती है। स्मृति के कारण सीखी हुई बात हमारे साथ रहती है। चित मन तथा अन्य तत्वों को आधार प्रदान करता है। योग दर्शन का सारा अनुसंधान ही चितवृतियों का निरोध करना है। चितवृतियों का निरोध करना ही चित को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हैं।
चेतना की तीन अवस्थाएं : 1. जागृत (जागृत अवस्था) 2. स्वप्न (स्वप्न अवस्था) 3. सुषुप्ति (गहन निद्रावस्था)। अन्तःकरण प्रथम दो अवस्थाओं में कार्य करता है। तीसरी अवस्था में वह निष्क्रिय रहता है। चित पर संस्कार होने के लिये कर्मेन्द्रियों से लेकर अंहकार तक के सभी करण सक्रिय और सक्षम होने चाहिये। ज्ञानार्जन के इन करणों को सक्षम बनाना, शिक्षा का कार्य है। अन्तःकरण चतुष्टय का परिष्कार करके आध्यात्मिक तत्वों को सरल, सुगम व बोधगम्यं बनाना शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य हैं।
निम्न प्रयोगों द्वारा अनतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है –
- इन्द्रियों की क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगाना।
- अच्छा साहित्य पढ़ना।
- षड्विकारों (काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर) को मन से निकालना।
- तप, दान, तयाग, ध्यान आदि में मन को लगाना।
- मन से कामनाओं का त्याग करना।
- सत्य मार्ग पर चलना।
- समदर्शी व निष्पाप होना आदि। अन्तःकरण की शुद्धि में सहायक होते हैं। अन्तःकरण के शुद्ध होने पर ही ईश्वरीय सत्ता का अनुभव होता है।
और पढ़े : भारतीय शिक्षा के आध्यात्मिक आधार – भाग दो (उपनिषद् एवं शिक्षा)
(लेखक आर्ष साहित्य के अध्येता है।)
